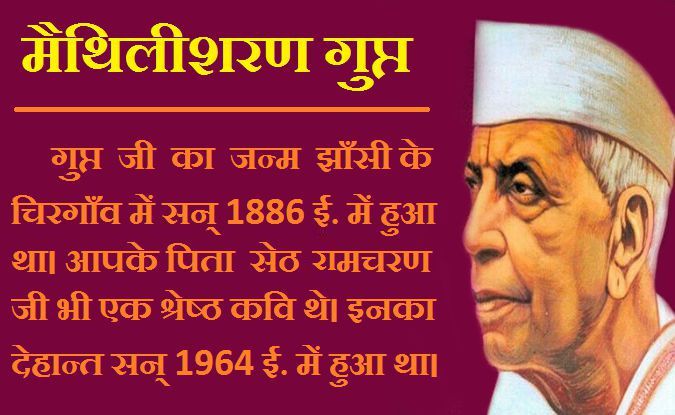Q. मैथिलीशरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन-परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए।
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त भारतीय संस्कृति के अमर गायक हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना का पवित्र आदर्श मिलता है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय जन-जागरण के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इनकी सेवाओं के लिए महात्मा गांधी ने इनको ‘राष्ट्रकवि’ की उपाधि से सम्मानित किया और राष्ट्रपति ने इनको संसद-सदस्य मनोनीत किया।
जीवन-परिचय
मैथिलीशरण गुप्त गुप्त जी का जन्म झाँसी के चिरगाँव में सन् 1886 ई. में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी भी एक श्रेष्ठ कवि थे। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद स्वाध्याय से ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में आए। महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया और जेल यात्रा की। साहित्यिक उपलब्धियों के कारण इन्हें आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों ने डी. लिट की मानद उपाधि दी। ‘साकेत’ महाकाव्य की रचना पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इनका देहान्त सन् 1964 ई. में हुआ था।
रचनाएँ
- इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं- १. साकेत, २. यशोधरा, ३. द्वापर, ४. भारत-भारती, ५. जय भारत, ६. पंचवटी, ७. झंकार, ८. जयद्रथ वध, ९. त्रिपथगा, १०. कुणाल गीत, ११. नहुष, १२. काबा और कर्बल, १३. विश्व वेदना, १४. विष्णू प्रिया आदि।
- इनके अतिरिक्त– १. चन्द्रहास, २. तिलोत्तमा और अनध गीति-नाट्य हैं।
- “१. वीरांगना, २. मेघनाद वध, ३. स्वप्नवासवदत्ता बंगला” संस्कृत और फारसी से अनुवाद की हुई रचनाएँ हैं।
इनकी कृति ‘भारत-भारती‘ में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान थी, उसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। भारत-भारती अपने समय की अत्यन्त लोकप्रिय रचना मानी जाती था। इसके गीतों से स्वतन्त्रता संग्राम सनानियों को पर्याप्त प्रेरणा मिली। इसकी कविता का एक नमूना देखिये –
वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है।
‘साकेत‘ नामक इनका महाकाव्य रामकाव्य परम्परा पर आधारित है। यह गुप्त जी की कीर्ति का आधार है। इसमें मर्मस्पशी स्थलों का अनुपम चयन और सरस चित्रण किया गया है। चित्रकूट प्रसंग एक ऐसा ही मार्मिक प्रसंग है जिसमें भरत के उज्ज्वल चरित्र की अभिव्यक्ति हुई है। कैकेयी का अनुताप भी उनकी मौलिक कल्पनाशक्ति का परिचायक है। उसका यह कथन अत्यन्त मार्मिक बन पड़ा है :
मुझ जैसे कीचड़ से भरत जैसे कमल का जन्म हुआ है, यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ‘यशोधरा‘
भी मैथिलीशरण गुप्त जी की उच्चकोटि की रचना है। इसमें गौतम बद्ध के गृह त्याग से लेकर ज्ञान-प्राप्ति तक की घटनाओं का समावेश है। इसमें विरहिणी गोपा की विकल स्थिति का वर्णन है। देखिए :
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।
हिन्दी साहित्य में स्थान
मैथिलीशरण गुप्त जी आधुनिक हिन्दी कविता के प्रतिनिधि कवि और राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाले राष्ट्रकवि के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी गुप्त जी को दिया जाता है उन्होंने यह दिखा दिया कि खड़ी बोली हिन्दी में भी वही माधुर्य, मार्दव एवं कोमलता है जो ब्रजभाषा की विशेषता समझी जाती थी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आपके बारे में सत्य ही लिखा है— “निःसन्देह आप हिन्दी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं।”
Q. “कैकेयी का अनुताप” के आधार पर कैकेयी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
अथवा
मैथिलीशरण गुप्त ने कैकेयी के चरित्र में जो नवीनताएँ उत्पन्न की हैं, उन्हें उदाहरण सहित समझाइए।
मैथिलीशरण गुप्त के रामकथा पर आधारित महाकाव्य साकेत में पारम्परिक रामकथा में कई परिवर्तन किए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख परिवर्तन है कैकेयी का पश्चाताप। गुप्तजी ने इस प्रसंग को साकेत के आठवें सर्ग में दिखाया है जिसे ‘कैकेयी का अनुताप’ शीर्षक से यहाँ संकलित किया गया है। भरत सारे समाज को लेकर राम को वापस अयोध्या लौटा लाने के लिए चित्रकूट गए जहाँ एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करत हुए स्वय को ‘कुमाता’ तक कहा डाला। वह यह भी सफाई देती है कि मैंने जो कुछ किया है, उसमें भरत का कोई हाथ नहीं है। अपनी बात के लिए शपथ खाती हुई वह कहती है:
पर, अबलाजन के लिए कौन-सा पथ है?
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ,
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ।
वह स्वीकार करती है कि मैंने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने पत्र को, राज्य का सुख देनें की कामना से यह अपराध किया। राम के समक्ष स्वयं को अपराधिनी मानती हुई वह कहती है-
सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना।
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया,
अपराधिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया।
वह कहती है कि मैं रघुकुल को कलंकित करने वाली रानी के रूप में जानी जाऊँगी और युगों-युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि कैकेयी ने अपने स्वार्थ के कारण राम जैसे पुत्र को वनवास दिया था। उसे सौ बार धिक्कार है :
रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी।
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा,
धिक्कार! उसे था महा स्वार्थ ने घेरा।
कैकेयी के इन पश्चाताप भरे हए शब्दों को सुनकर राम उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं :
जिस जननी ने है जना भरत सा भाई।।
जिस माता ने भरत जैसा भाई उत्पन्न किया है, वह धन्य है। प्रभु राम के कथन का समर्थन सारी सभा ने भी किया।
मैं पहाड़ जैसा पाप करके भी मौन रहूँ और राईभर भी अनुताप न करूँ, यह नहीं हो सकता। भला मन्थरा क्या कर सकती थी, दोष तो मेरा ही था, क्योंकि मैं अपने मन को ही काबू में न रख सकी। अब यह मन इस शरीर में मृत्युपर्यन्त जलता रहेगा और अपने पाप का दण्ड भोगेगा :
राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ?
कैकेयी कहती है कि मैं सारे दण्ड भुगतने को तैयार हूँ किन्तु कोई मुझसे भरत का मातृपद न छीने अभी तक लोग यही कहते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र निकल जाए पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती पर मैंने जो कुछ किया है उससे अब सब लोग यही कहेंगे कि माता भी कुमाता हो सकती है :
रे राम, दुहाई करूँ और क्या तुझसे?
उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चाताप की इस आग में जलकर कैकेयी निश्चय ही निष्कलंक और पवित्र हो गई है। गुप्तजी ने कैकेयी के इस अनुताप का समावेश ‘रामकथा’ में करके एक आवश्यकता की पूर्ति की है। कैकेयी ने मोह के वशीभूत होकर जो गलती की वह मानवीय दुर्बलता थी, किन्तु यह भी सच है कि जब किसी को अपनी भूल का पता चलता है तो पश्चाताप एवं प्रायश्चित के द्वारा वह अपने अपराध का परिमार्जन भी कर सकता है। गुप्तजी ने कैकेयी को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान कर एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। निश्चय ही साकेत का यह अंश अत्यन्त मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी बन पड़ा है।
Q. ‘साकेत’ में संकलित अंश के आधार पर उर्मिला के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए।
‘साकेत‘ मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित रामकथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें कवि ने रामकथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला को केन्द्र में रखकर कथावस्तु का निर्माण किया है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह-वर्णन कवि ने बड़े मनोयोग से किया है। उसके विरह वर्णन में मार्मिकता, सजीवता एवं विरह-व्यथित हृदय की टीस व्याप्त है।
शरद ऋतु का आगमन होने पर खंजन पक्षी दिखाई देने लगे हैं, धूप खिल गई है. सरोवर जल से भरे दिखाई दे रहे हैं और हंस उनमें क्रीड़ा कर रहे हैं। विरहिणी उर्मिला को शरद के रूप में अपने प्रिय के विभिन्न अंगों के दर्शन हो रहे हैं। वह अपनी सखी से कहती है :
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मनभाए।
फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए।
घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए।
इसी प्रकार शिशिर ऋतु के सारे उपादान विरहिणी उर्मिला को अपने तन में ही दिखाई पड़ रहे हैं। प्रकार वन-उपवन पतझड़ के कारण शुष्क हो गए हैं उसी प्रकार विरहिणी उर्मिला का शरीर विरह में सूख गया है। मुख एवं शरीर कुम्हला गया है। आँखें मोती रूपी आसू बरसाती रहती हैं। वह कहती है:
जितना मांगे पतझड दूंगी मैं इस निज नन्दन में।
कितना कम्पन तझे चाहिए ले मेरे इस तन में,
सखी कह रही पाण्डुरता का क्या अभाव आनन में।
विरहिणी उर्मिला को काम भावना भी सता रही है। वह कामदेव से कहती है कि मैं तो अबला हूँ और फिर वियोग व्यथा से पीड़ित हूँ। तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर प्रहार करो। यदि तुम्हें अपने रूप का गर्व है तो उसे मेरे पति पर न्योछावर किया जा सकता है और यदि तम्हें अपनी पत्नी रति के रूप का घमण्ड हो, तो लो मेरी चरण धूलि ले जाओ और उसे उस पर न्योछावर कर दो। इस प्रसंग को निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है:
मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो॥
होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न गारो।
मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो॥
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उर्मिला का विरह वर्णन गुप्त जी ने साकेत में बड़े मनोयोग से किया है। यह रामकथा में उनकी मौलिक उद्भावना है तथा रामकथा का एक मधुर प्रसंग है। गुप्तजी को इसमें पूर्ण सफलता मिली है यह निःसंकोच कहा जा सकता है।
हिन्दी साहित्य के अन्य जीवन परिचय
हिन्दी के अन्य जीवन परिचय देखने के लिए मुख्य प्रष्ठ ‘Jivan Parichay‘ पर जाएँ। जहां पर सभी जीवन परिचय एवं कवि परिचय तथा साहित्यिक परिचय आदि सभी दिये हुए हैं।